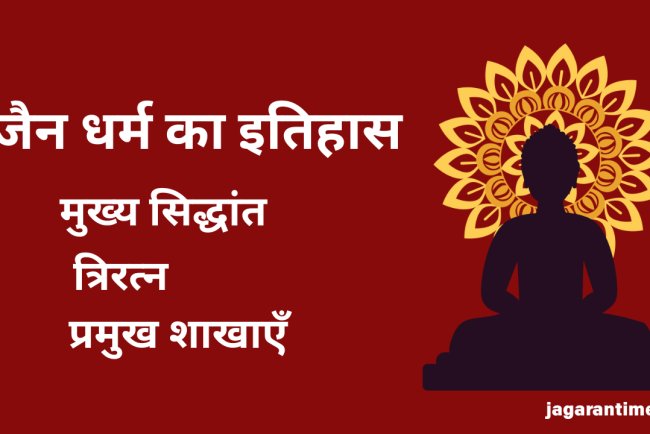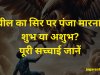पृथ्वी की आंतरिक संरचना: धरती के भीतर की रहस्यमयी दुनिया
जानिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रहस्यों को – भूपर्पटी, मैंटल और कोर की विशेषताएं, वैज्ञानिक अध्ययन और उनका जीवन पर प्रभाव।

हम जिस धरती पर रहते हैं, वह सतह से जितनी स्थिर और सधी हुई लगती है, उतनी ही जटिल और गतिशील उसकी आंतरिक संरचना है। पृथ्वी केवल एक ठोस गोला नहीं है, बल्कि इसकी परतें एक-दूसरे से भिन्न गुणों वाली हैं — तापमान, घनत्व, और संरचना के आधार पर। इस ब्लॉग में हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी परतें, उनकी विशेषताएँ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका महत्व।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे होता है?
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सीधा अध्ययन करना संभव नहीं है क्योंकि अभी तक हम कुछ किलोमीटर गहराई तक ही खुदाई कर पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves), ज्वालामुखीय गतिविधियों और गुरुत्वाकर्षणीय आंकड़ों की मदद से धरती के अंदर की जानकारी प्राप्त की है।
पृथ्वी की तीन मुख्य परतें
पृथ्वी को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है:
1. भूपर्पटी (Crust)
2. मैंटल (Mantle)
3. कोर (Core)
इन परतों की गहराई, घनत्व और रासायनिक संरचना अलग-अलग होती है।
भूपर्पटी (Crust)
यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं।
- गहराई: 5 से 70 किलोमीटर
- प्रकार:
- महाद्वीपीय भूपर्पटी: औसतन 35–70 किमी मोटी, ग्रेनाइट की बनी होती है।
- महासागरीय भूपर्पटी: औसतन 5–10 किमी मोटी, बेसाल्ट की बनी होती है।
- तापमान: सतह पर ठंडा, नीचे की ओर गर्म (~400°C)
- विशेषता: इसमें पर्वत, मैदान, महासागर आदि शामिल हैं।
यह परत पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का केवल 1% भाग बनाती है।
मैंटल (Mantle)
यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है और पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है।
- गहराई: लगभग 70 किमी से 2900 किमी तक
- तापमान: 500°C से 4000°C तक
- घनत्व: भूपर्पटी से अधिक
- संरचना: सिलिकेट खनिज, मैग्नीशियम और आयरन युक्त
- विभाजन:
- ऊपरी मैंटल (Upper Mantle): लगभग 670 किमी तक, इसमें 'एस्थेनोस्फीयर' नामक अर्धद्रव्यमान क्षेत्र होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स में मदद करता है।
- निचला मैंटल (Lower Mantle): 670 से 2900 किमी तक, अधिक कठोर और गर्म होता है।
मैंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% है।
कोर (Core)
पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा जो मुख्यतः लोहा और निकल से बना होता है।
बाह्य कोर (Outer Core)
- गहराई: 2900 से 5100 किमी
- तापमान: 4000°C से 6000°C तक
- स्थिति: द्रव अवस्था
- विशेषता: पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field) का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है।
आंतरिक कोर (Inner Core)
- गहराई: 5100 से 6371 किमी (पृथ्वी का केंद्र)
- तापमान: लगभग 6000°C
- स्थिति: ठोस अवस्था, उच्च दाब के कारण
- घनत्व: सबसे अधिक (~13g/cm³)
कोर पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 33% बनाता है।
भूकंपीय तरंगें और आंतरिक संरचना
भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली तरंगें — पी (P) और एस (S) तरंगें — पृथ्वी की अंदरूनी परतों से गुजरती हैं और वैज्ञानिक इन्हीं से यह पता लगाते हैं कि किस परत में क्या है। उदाहरण के लिए, S तरंगें द्रव में नहीं जातीं, जिससे यह साबित होता है कि बाह्य कोर तरल है।
पृथ्वी की परतों की तुलना
|
परत |
गहराई (किमी) |
अवस्था |
मुख्य तत्व |
विशेषता |
|
भूपर्पटी |
5–70 |
ठोस |
सिलिकेट |
सतह, मानव जीवन |
|
मैंटल |
70–2900 |
ठोस/अर्धद्रव |
Mg, Fe, सिलिकेट |
प्लेट गतियाँ |
|
बाह्य कोर |
2900–5100 |
द्रव |
लोहा, निकल |
चुम्बकीय क्षेत्र |
|
आंतरिक कोर |
5100–6371 |
ठोस |
लोहा, निकल |
सबसे गर्म भाग |
आंतरिक संरचना का जीवन पर प्रभाव
- प्लेट टेक्टोनिक्स: महाद्वीपों का विचलन, भूकंप, ज्वालामुखी इसी कारण होते हैं।
- मैग्नेटिक फील्ड: सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव करता है।
- भूगर्भीय खनिज: कोयला, लोहा, सोना जैसे खनिज परतों में पाए जाते हैं।
वैज्ञानिकों के प्रमुख योगदान
- मोहोरोविचिक असंतरण (Moho): क्रोएशियाई वैज्ञानिक आंद्रिया मोहोरोविचिक ने क्रस्ट और मैंटल के बीच की सीमा खोजी।
- गुटेनबर्ग असंतरण: मैंटल और कोर के बीच की सीमा।
- लेहमन असंतरण: आंतरिक और बाह्य कोर की सीमा।
आधुनिक तकनीक और अध्ययन
आजकल वैज्ञानिक 3D सिस्मिक इमेजिंग, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, और उपग्रह डेटा के माध्यम से पृथ्वी की गहराई का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में भी राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (NGRI) और ISRO इस दिशा में काम कर रहे हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना न केवल वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय है बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। भूकंप, ज्वालामुखी, खनिज संसाधन, पर्यावरणीय संतुलन — सब कुछ इस अदृश्य संरचना से प्रभावित होते हैं। यदि हमें धरती को बेहतर समझना है, तो उसकी परतों की गहराई में जाना ही होगा।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी हेतु है। इसमें दी गई वैज्ञानिक अवधारणाएं मान्य स्रोतों और अध्ययन पर आधारित हैं, फिर भी किसी विशिष्ट अध्ययन या निर्णय से पूर्व विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।