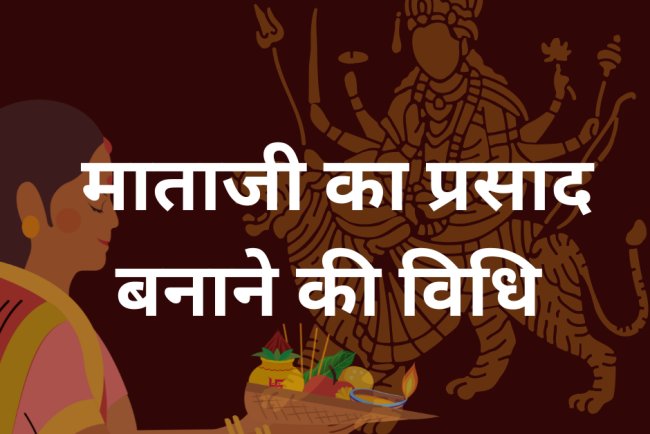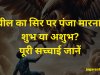डीआरडीओ की स्वदेशी तकनीक: समुद्री जल से मीठा पानी बनाने में बड़ी सफलता
डीआरडीओ ने समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। यह तकनीक तटरक्षक बल के जहाजों और तटीय इलाकों में जल संकट से राहत दिलाने में सहायक होगी।

भारत जैसे देश में, जहां जल संकट तेजी से विकराल रूप ले रहा है, वहां समुद्री जल को पीने योग्य मीठे जल में बदलना किसी वरदान से कम नहीं होगा। हाल ही में देश ने इस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल सकती है। यह तकनीक न केवल रक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी है, बल्कि देश के उन तटीय इलाकों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकती है, जहां पीने के पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है।
तकनीक का मूल आधार: पॉलीमर मेम्ब्रेन
डीआरडीओ की यह नई तकनीक ‘नैनो-पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमर मेम्ब्रेन’ पर आधारित है। यह उच्च-दाब पर समुद्री जल को छानकर उसमें से लवण, खनिज और अशुद्धियों को अलग कर देती है। इसके बाद जो पानी प्राप्त होता है वह पीने योग्य मीठा जल होता है। यह पूरी प्रक्रिया विलवणीकरण (Desalination) कहलाती है।
इस पॉलीमर मेम्ब्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत में ही विकसित किया गया है और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। इसे DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला “Defence Materials and Stores Research and Development Establishment” (DMSRDE) ने मात्र 8 महीनों में तैयार किया है। यह दर्शाता है कि भारत अब तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
तटरक्षक बल के लिए गेम चेंजर
इस तकनीक को विशेष रूप से भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों के लिए विकसित किया गया है। समुद्र में लंबे समय तक गश्त के दौरान पानी की आपूर्ति एक गंभीर समस्या बन जाती है। वर्तमान में जहाजों को पीने का पानी स्टोर करके ले जाना पड़ता है, जिससे वजन और स्पेस की समस्या होती है।
नई मेम्ब्रेन तकनीक के माध्यम से अब ये जहाज समुद्री जल को सीधे मीठे पानी में बदल सकते हैं और अपनी आवश्यकतानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि मिशन की अवधि भी लंबी की जा सकेगी।
सैन्य के साथ-साथ नागरिक उपयोग
हालांकि यह तकनीक पहले चरण में रक्षा क्षेत्र के लिए विकसित की गई है, लेकिन इसका भविष्य में नागरिक क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से तटीय गांवों और द्वीपों में, जहां पीने के पानी की भारी किल्लत है, वहां यह तकनीक जीवनदायिनी साबित हो सकती है।
भारत के कई समुद्री तटवर्ती राज्य जैसे गुजरात, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और पश्चिम बंगाल इस तकनीक के जरिए जल संकट से काफी हद तक निजात पा सकते हैं।
क्यों जरूरी है यह तकनीक?
भारत की एक बड़ी आबादी अब भी जल संकट से जूझ रही है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में समुद्री जल, जो कि असीमित है, को मीठे जल में बदलना ही एकमात्र दीर्घकालिक समाधान हो सकता है।
यह तकनीक पारंपरिक RO सिस्टम की तुलना में अधिक टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और लागत प्रभावी है। इसका रखरखाव भी अपेक्षाकृत आसान है और इसे दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से तैनात किया जा सकता है।
तकनीकी विशेषताएं
1. हाई-प्रेशर टॉलरेंस: यह मेम्ब्रेन उच्च दाब को सहन करने में सक्षम है, जिससे यह समुद्री जल को प्रभावी रूप से फिल्टर कर पाती है।
2. नैनो-पोरस संरचना: इसकी सूक्ष्म संरचना पानी में मौजूद छोटे से छोटे लवण को भी छान लेती है।
3. दीर्घकालिक उपयोग: यह तकनीक लंबे समय तक चलने वाली है और इसे बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती।
4. कम ऊर्जा खपत: यह प्रणाली ऊर्जा की खपत को न्यूनतम रखती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल बनती है।
भारत के लिए भविष्य का जल समाधान
समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। भारत के पास 7500 किमी लंबी समुद्री तटरेखा है और यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो देश के जल संकट को काफी हद तक हल किया जा सकता है।
भविष्य में सरकार इस तकनीक को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में तैनात कर सकती है। इसके अलावा, यह तकनीक आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, तूफान या युद्ध के दौरान भी बहुत उपयोगी हो सकती है।
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
डीआरडीओ की यह तकनीक अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर भी खरी उतरती है। इससे तैयार पानी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तय किए गए मानकों पर खरा उतरता है। यह भारत को जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई पहचान देगा।
ग्रामीण भारत में उपयोग की संभावना
ग्रामीण भारत में, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में, यह तकनीक एक क्रांति ला सकती है। स्थानीय स्तर पर मिनी प्लांट लगाकर लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा।
शिक्षा और जागरूकता की जरूरत
तकनीक के विकास के साथ-साथ इसके बारे में जागरूकता भी जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह इस तकनीक को लेकर जनता के बीच जानकारी फैलाए और इसे उपयोग में लाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करे।
आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम
यह उपलब्धि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत तकनीक के मामले में अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी बन रहा है।
डिस्क्लेमर:
इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। यह किसी विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विशेषज्ञ या विभाग से परामर्श अवश्य लें।