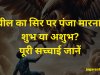भारत ने विकसित की विश्व की पहली जीनोम-संपादित धान की किस्में, अब इतना हो जाएगा प्रोडक्शन
भारत ने CRISPR-Cas9 तकनीक द्वारा विकसित विश्व की पहली जीनोम-संपादित धान की किस्मों को वाणिज्यिक स्वीकृति दी, जिससे उत्पादन में 20–25% वृद्धि संभव।

आज भारत ने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। देश की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी संस्थाएँ—विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग—ने मिलकर CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करते हुए विश्व की पहली जीनोम-संपादित धान की किस्में विकसित की हैं। इस अभिनव सफलता़ का उद्देश्य केवल किसानों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, जल संकट एवं भूमि क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों से मुकाबला करना भी है।
परिचय
धान (Oryza sativa) दुनिया भर में लगभग आधे मानव समाज के लिए मुख्य आहार है। बढ़ती आबादी, घटती कृषि योग्य भूमि और चरम मौसमी परिवर्तन के मध्य, धान की उत्पादकता में सुधार अपरिहार्य हो गया है। पारंपरिक तरीके से किस्मों का चयन और संवर्धन समय-साध्य होता है, और यह प्रक्रिया पर्यावरणीय और कीट-प्रतिरोधी लक्षणों की सीमित संख्या तक ही सीमित रहती है। जीनोम संपादन, विशेषकर CRISPR-Cas9 तकनीक, इस दूरी को काफी हद तक पाटता है।
जीनोम एडिटिंग क्या है?
जीनोम एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी पौधे या जीव के डीएनए पर सटीक परिवर्तन किए जाते हैं। पारंपरिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग (GMO) के विपरीत, यह तकनीक केवल लक्षित जीन पर ही काम करती है, जिससे अवांछित जीनों में बदलाव की संभावना न्यूनतम होती है। CRISPR-Cas9 एक “जीन-सकेंच” गियर की तरह काम करता है, जो वैज्ञानिकों को जीनोम में विशेष स्थलों को पहचानकर वहां चाही गई कटौती या परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है।
CRISPR तकनीक का योगदान
CRISPR-Cas9 की क्षमताएँ इसकी सरलता, तीव्रता और सटीकता में निहित हैं। शोधकर्ताओं ने पहले पौधों की जीनोम एडिटिंग पर प्रयोग किया था, लेकिन धान पर इसका अनुप्रयोग पारंपरिक प्रजातियों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। भारत के वैज्ञानिकों ने उच्च उत्पादकता, ड्राउट सहनशीलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जीनों को संशोधित और संयोजित करते हुए तीन प्रमुख किस्में (‘BGE-01’, ‘BGE-02’, ‘BGE-03’) तैयार कीं।
भारत में विकास का सफर
इस परियोजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब ICAR एवं DBT ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत किया। अत्याधुनिक शोध सुविधाओं एवं अनुभवी वैज्ञानिकों की टीम ने 3 वर्षों में लैब से खेत तक की यात्रा तय की। प्रारंभिक चरण में संवेदनशीलता और सुरक्षा परीक्षणों के बाद, 2023 में नियंत्रित फील्ड ट्रायल शुरू हुए। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन किस्मों को वाणिज्यिक उगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
विशेष किस्मों की विशेषताएँ
- उच्च उत्पादकता: पारंपरिक किस्मों की तुलना में 20–25% तक अधिक धान उत्पादन।
- ड्राउट सहनशीलता: कम पानी में भी खाद्यान्न उत्पादकता बनाए रखने की क्षमता।
- रोग एवं कीट प्रतिरोध: ब्लास्ट रोग, बकाया रोग तथा चावल पालक कीटों के खिलाफ प्रतिरोधक जीनों का समावेश।
- पोषक तत्व समृद्धि: जिंक और आयरन के स्तर में वृद्धि, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी पर्याप्त।
उत्पादन में अनुमानित वृद्धि
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन जीनोम-एडिटेड किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन में 1.5 टन की वृद्धि होगी। यदि देश भर में 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इन किस्मों का प्रसार होता है, तो कुल अतिरिक्त उत्पादन लगभग 15 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। यह मात्र अन्न आपूर्ति बढ़ाने का आंकड़ा नहीं; इससे किसानों की आय में भी औसतन 30–35% तक की बढ़ोतरी संभव है।
किसानों के लिए लाभ
1. कम इनपुट लागत: ड्राउट सहनशीलता के कारण सिंचाई के खर्च में कमी।
2. रोग प्रबंधन आसान: कम कीटनाशकों और रोगनाशकों की आवश्यकता।
3. उच्च बाज़ार मूल्य: पोषक तत्वों से समृद्ध धान की मांग निर्यात बाजार में भी बढ़ेगी।
4. आर्थिक सशक्तिकरण: बढ़ी हुई पैदावार से मिश्रित फसल मॉडल अपनाने की क्षमता।
पर्यावरणीय प्रभाव
जीनोम-संपादित किस्मों की ड्राउट सहनशीलता से जल स्रोतों पर दबाव घटेगा। कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों की खपत कम होने से मिट्टी और जल निकाय में प्रदूषण का जोखिम भी न्यूनतम होगा। इसके साथ ही, अधिक उत्पादन से जंगलों या अन्य संवेदनशील इकोसिस्टम में कृषि विस्तार की आवश्यकता घटेगी, जिससे जैव विविधता संरक्षित रहेगी।
सुरक्षा एवं नियमन
भारत में बायोटेक्नोलॉजी प्रसार एवं नियमन के लिए ‘जीएमसीबीआई’ (Genetic Modification and Biosafety Committee of India) ने कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन जीनोम-संपादित धान किस्मों को वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर जोखिम मूल्यांकन से गुज़ारना पड़ा। अब उत्पाद के समग्र मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है।
चुनौतियाँ
- समझ एवं स्वीकृति: कुछ उपभोक्ता और किसान जीनोम-संपादित फसलों को लेकर सतर्क हैं। जागरूकता अभियानों की आवश्यकता।
- वित्तीय एवं तकनीकी सहायता: छोटे किसान समूहों को बीज उपलब्ध कराने और तकनीकी मार्गदर्शन हेतु सरकारी व गैर-सरकारी योजनाएँ विस्तारित करनी होंगी।
- संसाधन एवं बौद्धिक संपदा: शोध संस्थानों और बीज कंपनियों के बीच लाभ साझा करने पर पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक।
भविष्य की संभावनाएँ
जीनोम एडिटिंग एक सीमित उपकरण नहीं, बल्कि कृषि क्रांति की नींव बन सकता है। चावल के अलावा अन्य अनाजों जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा दलहन फसलों में भी इसी तकनीक का विस्तार संभव है। देश में ‘प्रधानमंत्री सुजलाम सुफलों’ अभियान के अंतर्गत जल संकट से जूझ रहे राज्यों में इन किस्मों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
भारतीय वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि न केवल देश के खाद्य संप्रभुता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी सुनहरा अध्याय जोड़ेगी। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह जीनोम-संपादित धान की किस्में किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण तीनों के लिए अवसर और सुरक्षा दोनों प्रदान करती हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण):
यह लेख केवल शैक्षिक एवं जानकारीगत उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। कृषि संबंधी निर्णय लेने से पहले कृपया कृषि विज्ञान विशेषज्ञ या संबद्ध सरकारी/निजी संस्थानों से परामर्श अवश्य करें।